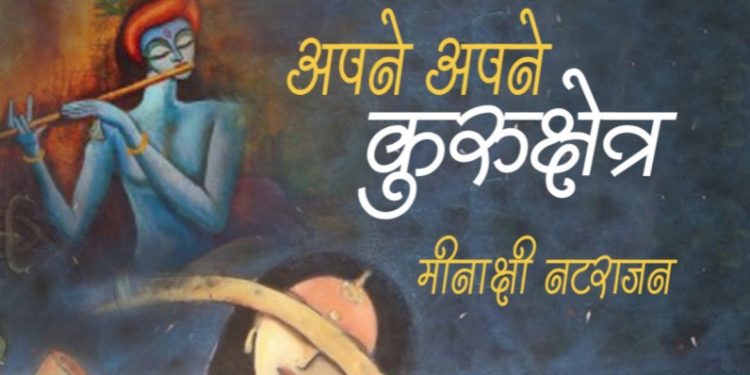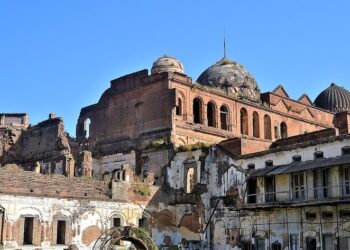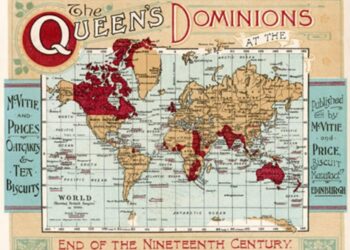नई रचना के लिए प्रेरणा देने का जैसा काम भारत में ‘महाभारत’ ने किया है, शायद किसी और रचना ने नहीं.
महेश दर्पण
भारतीय संस्कृति के इस आधार ग्रंथ में कथा के जितने तार्किक रूप मिलते हैं, वे अन्यत्र दुर्लभ हैं. संभवतः इसी कारण कहा गया होगा कि अब जो भी श्रेष्ठ रचा जाएगा, महाभारत उसका उपजीव्य होगा. यह सच भी साबित हुआ क्योंकि भारत की प्रायः सभी भाषाओं में ‘महाभारत’ से प्रभावित रचनाएं कालांतर में अनेक लिखी गईं. क्यों न लिखी जातीं, आखिरकार जो महाभारत में नहीं है, वह कहीं नहीं है!
यह सब उल्लेख करने का विचार आने का कारण है- मीनाक्षी नटराजन का उपन्यास ‘अपने-अपने कुरुक्षेत्र’. इस उपन्यास में वह अंतस के रणक्षेत्र की खोज कर, कथा का ताना-बाना तैयार करती हैं. ठीक कहा है भूमिका में उन्होंने, ‘‘हर मनुष्य का मन रणक्षेत्र ही तो होता है. जहां वह निरंतर जूझता है. अनेक प्रकार की ग्रंथियों, ़द्वंद्व, असमंजस, संबंधों को लेकर ऊहापोह का नित्य प्रति सामना करता रहता है. एक द्वंद्व से निकलते-निकलते दूसरे में फंस जाता है. महाभारत के हर चरित्र ने अपने-अपने मनक्षेत्र में जीवनपर्यंत ऐसे ही अनगिनत संग्राम का सामना किया. महाभारत का युद्ध न तो कुरुक्षेत्र में आरंभ हुआ और न ही उसका अंत वहां हुआ. वह तो केवल भौतिक स्थल क्षेत्र था. युद्ध तो मैदान से बहुत पहले मनक्षेत्र में आरंभ हो गया था.’’
मनक्षेत्र के उद्वेलन के तापमान के अनुरूप छह पात्रों के अंतस में चल रहे कुरुक्षेत्र के माध्यम से कथा कहने के लिए मीनाक्षी नटराजन ने क्रमशः छह अध्याय सत्यवती, गांधारी, कुन्ती, शिखंडी, द्रौपदी व भीष्म पर आधारित बनाए हैं. यहां कुछ प्रश्न उठाती सत्यवती हैं, प्रतिज्ञाबद्ध गांधरी हैं, जीवन-प्रवाह में कुन्ती हैं, प्रतिशोधयुक्त शिखंडी हैं, प्रणकृत द्रौपदी हैं और प्रयाण की ओर भीष्म हैं. प्रथम पांच अध्यायों में चार स्त्री व एक पुरुष पात्र भीष्म के पास आ, संवादों के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाते हैं. केवल अंतिम अध्याय में भीष्म-कृष्ण संवाद से कथा को समाहार मिलता है. इन संवादों की विशेषता यह है कि ये पात्रों की मनःस्थिति के अनुरूप आकार स्वतः ग्रहण करते चले गए-से लगते हैं. कहने में अत्यंत सरल-सा यह वाक्य औपन्यासिक रचना के लिए अत्यंत श्रम और संवेदनशील मन की अपेक्षा रचनाकार से करता है. यदि ऐसा न होता, तो संभवतः मीनाक्षी इतना पठनीय उपन्यास न दे पातीं.
प्रायः प्रत्येक अध्याय की यह विशेषता है कि कथारंभ में ही कथा एक आलाप लेती प्रतीत होती है. कहीं यह प्रकृति के साथ हस्तिनापुर के राजप्रसाद का चित्र खींचती है तो कहीं सांध्यबेला को साकार कर देती है. कहीं भोर सामने है तो कहीं युद्ध के परिणाम, कहीं रात्रि के तीसरे प्रहर में अस्थिर मन भीष्म हैं तो कहीं असीम आनंद में उनका अंत. यहां भाषा में धैर्य व सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति के कारण अध्याय की एक कथा-भूमि बनने लगती है. वह प्रारंभ और अंत में समान स्थैर्य लिए है. संवादों की इस उपन्यास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है.
राजमाता सत्यवती व भीष्म के संवाद पर आधारित पहले अध्याय में आज भी प्रासंगिक यह धारणा उल्लेखनीय है कि ‘‘यदि मान्यताओं को समयानुसार बदला नहीं गया, परिमार्जित नहीं किया गया तो वे अनायास ही अपनी रचनात्मक आद्रता को खोने लगती हैं. धीरे-धीरे उनकी मौलिकता सूखने लगती है.’’ उपन्यास समीचीन सत्य प्रस्तुत करता है- प्रकृति की तरह वसंत के आगमन पर ही नई मान्यताएं प्रस्फुटित होती हैं.
सत्यवती प्रश्नों से भरी हैं, अपने ही प्रति नहीं, दूसरों के प्रति भी जो उनके जीवन को प्रभावित करते रहे हैं और भीष्म को अपने प्रश्नों के घेरे में लेती हैं. अनायास हुए इस संवाद में उठ आए प्रश्न विचार को बाध्य करते हैं. प्रश्न उठता है कि स्त्री के चरित्र को यौन शुचिता तक ही सीमित क्यों रखा गया है? क्या उसके मन की पवित्रता का कोई मोल नहीं? इसके विपरीत पुरुष, वह भी यदि ऋषि है, तो महान मान लिया जाएगा! अपने भीतर युद्धरत प्रश्नों को वह बाहर निकालती है और भीष्म को पिता की शर्तें मान लेने के लिए आश्चर्य का कारण बताती है. एक मत्स्य कन्या के सामने होने वाले पति की आयु का कोई अर्थ नहीं, प्रतिष्ठा-प्रभाव ही प्रमुख क्यों रहा?
प्रश्न उठाती कथा पूछती है कि भीष्म भी क्यों पितृसत्तामक समाज का अंग बना रहा, क्यों उसने कभी ऐसी चेष्टा नहीं की कि सत्यवती के मनोभावों को भी जानने की प्रक्रिया सामने हो पाती! अच्छा यही है कि यहां भीष्म का आत्म-स्वीकार खुलता है कि उन्होंने नारी के स्त्री रूप को नहीं पहचाना! बगैर नियम-परंपरा को परखे पालन करने वाले भीष्म की आलोचना के बीच भी कथा में भीष्म का चिंतन आकार लेता है- धर्म क्या है? सत्य का पालन कैसे हो?
ऊंचे आदर्शों के बरक्स, पहली बार औपन्यासिक ढांचे में जीवन के कटु यथार्थ से उभरी वह सच्चाई सामने हो आती है जिसमें सत्यवती का अतीत विचार का विषय बनता है. अनौपचारिक परिवेश से आयी सत्यवती प्रासाद में कैसी असहजता झेलती रही, किसी ने न सोचा. जीवन को यदि नियति ही संचालित करती है, तो स्त्री के प्रति वह इतनी क्रूर क्यों है? उसे प्रायः स्मरणीय बनाकर उसके जीवन की सहजता ही छीन ली जाए, तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ है? विवाहित स्त्री-पुरुष की स्थिति में भेद क्यों होता है? विवाह की कोई भी पहचान, स्त्री की तरह पुरुष क्यों धारण नहीं करता? नारी-स्वाभिमान की रक्षा के समक्ष भीष्म हस्तिनापुर की भक्ति में क्यों डूब जाते हैं? सीधी व सधी भाषा में सत्यवती अपने प्रश्नों से भीष्म को निरुत्तर कर देती हैं. पर सीख छोड़ जाती हैं कि कुल और राज्य की स्त्रियों के सम्मान और मर्यादा का विशेष ध्यान रखना. धर्म के सही स्वरूप को पहचानने की सीख भी सत्यवती जाते-जाते भीष्म को दे जाती हैं. यही कारण है कि इस अध्याय के अंत में भीष्म सत्यवती के प्रश्नों के साथ अकेले रह जाते हैं.
दूसरा अध्याय है ‘गांधरीः प्रतिज्ञा’ का. यह वह चरित्र है जिसका भीष्म से कभी संवाद नहीं रहा. पुत्रों की तामसिक प्रवृत्ति की कालिमा लिए, द्यूत सभा में हुए अन्याय का अंधेरा लिए, आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी ज्येष्ठ पिताश्री से मिलने चली आई हैं. उनकी गलती उपन्यास-कथा यह बताती है कि बेटों को अनुशासन में बांधने की जगह, वह खुद आंखों पर पट्टी बांधे हैं. यह कथा में चरित्रों का अपनी दुर्बलता के साथ खुलना है. इसके परे भीष्म भी नहीं, वह इस महाभारत के केंद्रीय चरित्र भले हों, न्यूनताएं उनमें भी हैं!
वह अपमानित होती स्त्री की मर्यादा को संरक्षण न दे पाने के कारण दुखी हैं, पर संकल्प से बंधे हैं. जबकि उनके बरक्स गांधारी द्रौपदी के साथ हुए अन्याय की गहरी पीड़ा महसूस करती है. कथा संकेत करती है कि इसके बावजूद यदि उसमें कठोरता बनी हुई है, तो उसका कारण संभवतः शकुनि है.
इस संवाद में, भीष्म के साथ उसका स्वर क्षमा का है. वह अपना अतीत पितृकुल की परिस्थितियां सामने रखते हुए खोलती है. यहां पता लगता है कि शकुनि को द्यूत क्रीड़ा विरासत में मिली है. यह वह परिवार था जहां मां मरने तक पिता का मुंह नहीं देखना चाहती. महाराज भी मां के मरने पर नहीं आते. यह कठोरता परिवार के स्वभाव की जड़ों में है. द्यूत महाराज सुबल को निर्बल करता जा रहा है. संवाद कुछ लंबे, पर सोद्देश्य हैं. भीष्म उनमें पहली बार गांधारी के यथार्थ से परिचित हो रहे हैं. वह सिर्फ सुन रहे हैं.
खल शकुनि के चरित्र की कुंजी इस रूप में यहां खुलती है कि वह दरअसल नियंत्रण चाहते हैं. कहीं सब कुछ फिसल न जाए! यहां भी भीष्म का गंभीर चिंतन सामने है. कथा में एक तनाव अवश्य है, पर गांधरी से जुड़ी झूठी कथाएं एक्सपोज करती है स्वयं वह. सच सामने आता है कि कैसे गर्भवती के साथ महाराज काम संबंध करते रहे. दांपत्य की सूक्ष्मताएं कितनी निर्भम होती हैं. पूरे इस कथा-समय में सबकी आंखों पर कोई न कोई पट्टी बंधी नजर आती है. इससे अलग बस कृष्ण व विदुर ही नजर आते हैं.
कथा का स्वरूप कुछ ऐसा है कि वह नातिविस्तार शैली धारण कर चलता है. संकेत हैं और उनमें खुलती सच्चाइयां. अध्याय में गांधारी के आगमन का सच यह है कि वह य़ु़द्ध को अधिकाधिक टालना चाहती है. भीष्म के पास सिवाय इस सदिच्छा के कुछ नहीं कि वह संकल्प से मुक्ति की कामना करें.
भीष्म हर किसी के लिए आदरणीय हैं, इसलिए युद्धपूर्व स्थितियों में उनकी भूमिका को सभी महत्वपूर्ण मान कर चलते हैं. पुत्र वधू कुन्ती स्वयं इसी भाव से, नित्य गंगादर्शक भीष्म से मिलने चली आयी है. कथा का यह तीसरा अध्याय बताता है कि कर्ण के प्रति गहरी संवेदना है भीष्म में. उनमें कुन्ती का यह संवाद पिता की तरह है. उपन्यास की कतिपय अन्य स्त्रियांे की तरह कुंती भी मायके से ससुराल में किसी नए पौधे की तरह रोंपी गई है. अब वह चाहती है कि उसे, पुत्रों व द्रौपदी को अधिकार मिलें, अनुकंपा नहीं. कुन्ती का चरित्र अपने अतीत में दुर्वासा के साथ संसर्ग प्रसंग में नियोग और अविवाहित मातृत्व की पीड़ा लिए है. यहां भी उसे जीवन के यथार्थ से संघर्ष की प्रेरणा धाय मां से मिलती है, जो कुंती के शिशु को उससे अलग कर नवजीवन प्रदान करती है.
यहां वर्तमान में सिर उठाता अतीत है और उसके श्रोता भीष्म का मंथन. यहीं भीष्म को स्त्री-पीड़ा न समझ पाने की तकलीफ के कारण, अपने ही संकल्प पर प्रश्न उठाने पर विवश होता देखा जा सकता है. पांडु-कुन्ती विवाह का मूल कारण बनता है हस्तिनापुर क्योंकि वहां कुन्ती की पूर्व संतान है. पर यह पांडु का दूसरा विवाह है. कुंती के साथ उसकी कथा गुप्त चली आई है. उसे धाय मां का परामर्श जो मिला है. यही कारण है कि कुन्ती आवरणों में जीना सीख गई है. वही पांडु को किदंम द्वारा दांपत्य सुख से वंचित रखने की कथा किंवदंती रूप में प्रचलित करने का भेद खोलती है. यहां फिर नियोग की नौबत सामने हो आती है. बड़ी बात यह है कि कुन्ती का सच जानते हुए भी विदुर और भीष्म, गुप्त ही रखते हैं.
स्त्री ही इस उपन्यास में स्त्री के साथ खड़ी मिलती है. द्रौपदी के पक्ष में खड़ी कुंती का विवेक सामने आता है. पर यहां वह भीष्म के पास महज इसलिए आई है कि कर्ण को य़ुद्ध करने से रोकने का आग्रह कर सके. वह जानती है कि विलंब ही उसकी आयु को बढ़ा सकता है. जिसे भीष्म आकार दे सकते हैं. भीष्म चूंकि भविष्य से परिचित हैं, इसलिए कथांत में उनका हाथ कुंती के सिर पर दिखना एक नाट्य भर है. सत्यवती और गांधारी के उपरान्त भीष्म से कुन्ती की यह भेंट भी कम मार्मिक नहीं है.
चैथे अध्याय में शिखंडी भीष्म से आकर मिलें, इससे पूर्व अनायास यह सूचना आती है कि महाभारत के य़ु़द्ध का यह दसवां दिवस है. सर्वश्रेष्ठ योद्धा होते हुए भी भीष्म घायल हो चुके हैं. स्त्री पर शस्त्र न उठाने की उनकी प्रतिज्ञा के बीच, क्लीव शिखंडी का सामने हो आना इसका कारण है. इसी कारण अर्जुन बाणों की बौछार का अवसर पा जाते हैं.
उपन्यास की कथा का मर्म यह है कि युद्ध भूमि के बाहर शत्रु पक्ष को भी मानवीय दृष्टि से देखते हैं योद्धा. यही कारण है कि पांडवों सहित सभी भीष्म की इस स्थिति पर दुखी हैं. ऐसे में शिखंडी स्वयं उनसे मिलने जाता है जो भीष्म के लिए आत्मबोध की स्थिति बन जाती है. उन्हें शिखंडी की ओर से आभास करा दिया जाता है कि युद्ध में भले ही स्त्री पर प्रहार न करना हो, पर अनेक अवसरों पर स्त्रियां भीष्म के प्रहार ही तो सहती रही हैं. सीधा प्रश्न खड़ा है उनके समक्ष कि स्त्री उनके लिए दुर्बल है य़ा तुच्छ और हीन?
शिखंडी के बहाने भीष्म को अनेक स्त्रियों की कथा स्मरण हो आती है. बेटी के रूप में जन्मी, पर क्लीव बन गई शिखंडी की कथा बताती है कि मां तो उसे झूठे ही पुत्रवत पालती रही. यहां तक कि उसका विवाह तक कररा दिया जाता है… तब कहीं खुलती है समाज की क्रूरता. यह एक व्यक्तित्व की अपनी पहचान ही छिपा लेने की त्रासदी है. भीष्म को स्मरण हो आई है अम्बा. वे उसके भी अपराधी जो हैं. शिखंडी प्रसंग में बस वासुदेव हैं, जिनकी भूमिका न्यायपूर्ण है. वही शिखंडी को गरिमापूर्ण जीवन में लौटाते हैं. महाभारत की कथा से उपजी किंवदंती में दम नजर आता है कि अंबा ने ही प्रतिशोध के लिए शिखंडी के रूप में जन्म लिया. अंबा के कथन का सही अर्थ खुलता है कि भीष्म का पुरुषोचित अहं एक दिन अपनी पराजय स्वीकार करेगा. स्त्री के समक्ष अपने शस्त्र के रूप में भीष्म अपना दंभ समर्पित कर देंगे. अच्छी बात ये है कि क्षमा मांगते भीष्म का स्वर कहता है कि एक दिन संसार प्राणी मात्र की गरिमा पर विचार करेगा. इस अर्थ में आज चल रहे किन्नर या थर्ड जेंडर विमर्श का मूल भी महाभारत में है. शिखंडी के बहाने वहां इसका निष्कर्ष समाज की खोखली सोच और आडंबर को एक्सपोज करना है.
उपन्यास का पांचवा अध्याय ‘द्रौपदीः प्रण’ है. यह युद्ध के सोलहवंे दिन की समाप्ति पर प्रारंभ होता है. अभिमन्यु के न रहने के बाद द्रौपदी युद्ध क्षेत्र में यह सोचती आई है कि उसने, सुभद्रा ने और उत्तरा ने युद्ध में कैसा मूल्य चुकाया? इस स्थिति में उसे वासुदेव की शिक्षा याद हो आती है कि व्यक्तिगत प्रतिशोध को युद्ध का निमित्त न बनाओ. पर द्रौपदी में तो प्रतिरोध का माद्धा द्यूत सभा से ही चला आ रहा है. उसे स्मृतियों में बीता समय सामने हो आता है. स्वयंवर के कटु दृश्यों में स्मरण है कर्ण का अपमान.
द्रौपदी-भीष्म संवाद खासा लंबा है. द्रौपदी की विचार शृंखला एक मां जैसी है. यह स्वाभाविक है. पर वह एक स्त्री की तरह भी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि युद्धोपरांत विषाद परिवारों की स्त्रियों के लिए है. वह अपनी जीवन-यात्रा की ओर मुड़कर देखती है. पाती है कि उसे तो अपनी पावनता और पांच पतियों के प्रति समता को निरंतर सिद्ध करना था. युद्ध की छाया से द्रौपदी को बाहर निकालने के लिए भीष्म द्रौपदी को वासुदेव से मिलने को कहते हैं. वह स्पष्ट करते हैं- ‘‘तुम न तो मानवता की इस गति का निमित्त बनी हो और न ही यह युद्ध तुम्हारे कारण लड़ा जा रहा है. वासुदेव से मिलकर ही तुम्हारे अशांत शोकाकुल चित्त को शांति मिलेगी.’’
हर घटना के तर्कों को रचनाकार ने बड़ी खूबसूरती से इस लद्यु उपन्यास में पिरोया है. यहां तक कि कर्ण को स्वयंवर में न चुने जाने के पीछे वासुदेव की सोच भी. उन्हें आशंका थी कि कर्ण द्रौपदी को, अपने मित्र दुर्योधन को सौंप सकते थे. यहां भीष्म के प्रश्न परेशान करने वाले हैं- ‘‘क्या तुम्हें यह वैवाहिक संबंध असहज नहीं लगा?’’ इसका उत्तर द्रौपदी बड़ी सहजता से देती है- ‘‘वह निर्णय मेरा था.’’
कथा में उल्लेखनीय यह है कि भीष्म द्रौपदी के मन में कुन्ती के प्रति आदर देख रहे हैं. द्रौपदी वासुदेव का वह कथन स्मरण कर रही है जिसमें कहा गया था कि समाज को अपना न्यायधीश मत बनने देना. यह आज भी प्रासंगिक है. अन्य अध्यायों की तरह यहां भी भीष्म से संवाद करती द्रौपदी अपनी वेगवान कथा प्रथम पुरुष में कह और स्मरण कर रही है. वह संघर्षों के मध्य अपने समक्ष आई चुनौतियों को भी सहज ही कह जाती है- ‘‘मेरी चुनौती यह थी कि पांड़व पत्नियों को, मुझे लेकर असुरक्षा की अनुभूति न हो. यहां तक कि वह यह सच भी खोल देती है कि पांडव पत्नी के रूप में उसने क्रमशः एक-एक वर्ष एक-एक के साथ व्यतीत करने का निर्णय लिया था. वह भीष्म के समक्ष खुलकर संवाद करती है. यहां तक कि अपने और धर्मराज के एकांत को फाल्गुनी द्वारा भंग करने की घटना भी नहीं छिपाती. यही नहीं, वह सभी पांडवों की विशेषताएं भी बता देती है. इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों का निर्मल भाव ध्यान देने योग्य है. द्रौपदी को यह बताने में भी कोई गुरेज नहीं कि सुभद्रा-पुत्र होते हुए भी क्यों अभिमन्यु उसका अधिक आत्मीय था. सच है कि द्रौपदी की तर्कशीलता का सर्वश्रेष्ठ रूप द्यूत सभा में ही खुलता है, जहां भीष्म निरुत्तर हो गए थे. जबकि आज वह क्षमा मांगते हैं.
पूरे उपन्यास में द्रौपदी सर्वाधिक प्रासंगिक और स्पष्ट लगती है, जब वह कहती है कि हमारे पारिवारिक ताने-बाने में हम न तो पुत्रों को सही शिष्टाचार और मान सिखाते हैं, न ही पुत्रियों को सचेत, सजग और आत्मनिर्भर बनाते हैं. वह साफ कहती है- ‘‘मेरा प्रण कहां पूरा हुआ? वह तो तब तक अधूरा है, जब तक समाज की वृत्ति नहीं बदल जाती. एक दुःशासन के दैहिक अंत से क्या होगा? हर नारी को तब तक संघर्ष करना पड़ेगा, जब तक कि समाज का वातावरण ऐसा न हो जाए कि फिर कोई दुःशासन किसी का केश और वस्त्र न खींच पाए.’’
वह भविष्य में कोई प्रण न करने की बात इसलिए कहती है कि हर प्रतिशोध की ज्वाला किसी स्त्री को आहत करती है. इस अध्याय में यक्ष-प्रश्नों के मध्य अवचेतन मानस का दृश्य अद्भुत है. द्रौपदी निजी भवितव्य की चिंता न करने के जिस नोट पर यह अध्याय संपन्न करती है, वह अपने कर्म में प्रवृत्त होने का संदेश देता है. संबल कृष्ण तो हैं ही.
अंतिम अध्याय ‘भीष्म: प्रयाण’ के शीर्षक से भले ही हो, यह उपन्यास प्रारंभ से अंत तक भीष्म के धागे में बंधा रहा है. सत्यवती हो चाहे गांधारी, कुंती हो चाहे द्रौपदी या शिखंडी, सभी भीष्म से आकर मिलते और संवाद करते हैं. सभी के प्रश्न भीष्म से हैं. भीष्म इस समूचे उपन्यास में कृष्ण के साथ होते हुए भी केंद्रीय चरित्र बन गए हैं.
उपन्यास बताता है कि घायल अवस्था में लेटे-लेटे भीष्म को आठ दिन हो चुके हैं. यह अठारहवां दिन है जब वह दुर्योधन वध की सूचना पाते हैं. अब विश्वास है उन्हें कि युधिष्ठिर अवश्य धर्मराज्य स्थापित करेगा. कथा धारा बताती है कि भीष्म कुछ अस्थिर मन हैं. तभी परिचारक द्वारा सूचना दी जाती है कि पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा ने प्रतिशोधवश आग लगा दी. ऐसे में वासुदेव का आगमन क्या होता है कि उनके साथ भीष्म का ऐसा संवाद प्रारंभ होता है जिसमें जीवन का सार ही प्रस्तुत हो जाता है.
भीष्म उनसे इस जन्म के प्रवास से मुक्ति मांगते हैं, तब वासुदेव सीख देते हैं- ‘‘क्या मुक्ति किसी के द्वारा कभी प्राप्त हो सकती है?’’ वह भीष्म को अपने मन को बंधनों के भंवर में डूबने से बचाने को कहते हैं. मुक्ति को वह मनुष्य के ही भीतर बताते हैं. वह भीष्म के भ्रमों का निवारण करते हैं. कहते हैं- आपने जीवन भर के लिए अपने को संकल्पों के पाश से बांध लिया, उसका दंभ पाल लिया. जबकि भीष्म को भ्रम था कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का स्थूल रूप में पालन किया है.
कृष्ण के संवाद में जीवन-मरण का यथार्थ खुलता जाता है. वह स्पष्ट कर देते है कि उन्होंने किसी को मुक्त नहीं किया. भय की बेड़ियों में जकड़ा समाज स्वयं दास हो जाता है. भय यह है कि लोग क्या कहेंगे? वह पूतना-प्रसंग की नवीन व्याख्या करते हैं. बच्चे न रहने से वह किसी भी बच्चे को दूध पिलाने क्या दौड़ पड़ती है, सभ्य समाज पत्थर मारकर उसे डायन घोषित कर देता है. प्रचारित करता है कि उसका दूध विषाक्त है. पूतना चोरी से कृष्ण को स्तनपान कराती है, वह तृप्त भाव से पीते हैं तो पूतना का कलंक मिट जाता है. उसकी विक्षिप्तता जाती रहती है. उपन्यास संकेत करता है कि नन्हे शिशु को सुविधा से अधिक स्नेह की आवश्यकता होती है. उसे संरक्षण मात्र से संतोष नहीं हो पाता. कृष्ण बोध कराते हैं कि मनुष्य स्वयं को पहचानता नहीं, इसलिए सोचता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं. उसे सर्वप्रथम स्वयं को बंधन मुक्त करना पड़ता है.
बड़े संजीदा ढंग से यह उपन्यास सभ्यता व समाज की आलोचना करता है. माध्यम बनते हैं कृष्ण. इस अध्याय में सीधा संवादों से और अन्यत्र संकेतों में. उपन्यास स्पष्ट करता है कि शक्ति संपन्न वर्ग जन सामान्य को ठगता है. वह उसके भोले पन को अंधश्रद्धा में परिवर्तित कर देता है. कृष्ण भय के विविध रूप खोलते हैं. स्पष्ट करते हैं कि हमें अपने संचित को खोने का भय सताता है. अधिक संग्रह से होड़ की प्रवृत्ति पनपती है.
कृष्ण प्रेम को सही रूप में परिभाषित करते हैं. बताते हैं कि वहां कुछ पाने की अभिलाषा नहीं है. मोह और आसक्ति से तो भय पैदा होता है. वह धर्म के मार्ग पर भी टिप्पणी करते हैं- वह एकांगी होता है. उसका पक्ष लेने पर व्यक्ति अपने परिवार को खो देता है कई बार. सोचना चाहिए कि परिवार तो व्यापक सृष्टि है. यही कारण है कि बलराम को कृष्ण की प्रताड़ना मिलती है. वह किसी भी कर्म को हेय दृष्टि से न देखने को कहते हुए बताते हैं- इससे उसकी क्रिया में ऐसे आनंद की अनुभूति होती है कि आप के ‘स्व’ का नाश होने लगता है.
वह अपनी आठ पत्नियों की विशेषताएं भीष्म के पूछने पर खोलते चले जाते हैं. कृष्ण के लंबे संवादों में, भीष्म बस एक श्रोता बने लगते हैं. कृष्ण अपने समय के साथ ही, अपने प्रिय अर्जुन की भी आलोचना करते नजर आते हैं. स्वयं की भूमिका वह युद्धोपरांत, आहों को समेटने की पाते हैं. उन्हें करुणा का लेप लगाना है.
कृष्ण के संवाद का स्वरूप ही ऐसा है कि भीष्म तृप्त हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि वे अब मुक्त हो सकते हैं. उन्हें भान हो जाता है कि वह मिथ्याभिमान के आधिपत्य को न रोक सके. अपने ही भीतर परमात्मा के अंश को न पहचान पाए. वासुदेव में उन्हें दिव्य का साक्षात्कार हो जाता है.
उपन्यास का केंद्र भीष्म ही हैं, अतः उपन्यास का समाहार भी यही अनुकूल लगता है. यह एक सुखद सच है कि इतिहासकार मीनाक्षी नटराजन ने ‘अपने अपने कुरुक्षेत्र’ रचकर एक सिद्धहस्त उपन्यासकार होने का परिचय दिया है. इस उपन्यास से ‘महाभारत’ की एक और मन भूमि खुली है जहां अनेक कुरुक्षेत्र हुए हैं. इसके पात्र अपनी समूची बेलाग मुद्रा में सामने हैं. न छिपाते हैं कुछ और न छिपना चाहते हैं. वे बस यह चाहते हैं कि समय भूमि में उनका सच सबके सम्मुख हो आए, ताकि वे स्वयं की नजरों में अपराधी न बने रह जाएं. यह कथा में यथार्थ की ऐसी पड़ताल है जहां जीवन की कटु सच्चाइयां प्रथम पुरुष में सामने हो आती हैं.
इन सचाइयांे को यदि पाठक महाभारत काल तक ही सीमित न करेंगे, तो उन्हें इस कथा के वर्तमान प्रासंगिकता के अर्थ भी खुलते नजर आने लगेेंगे. इस उपन्यास की सार्थकता यही है कि यह अंधेरों में घुटने के बजाय प्रश्नांकन पर विश्वास रखती है, जो भारतीय जीवन-धारा का एक अनिवार्य पहलू रहा है. जिस दिन प्रश्नों पर रोक लगने लगेगी, हमारे समाज की पारंपरिक विचार-प्रक्रिया में गतिरोध पैदा होने लगेंगे. जिन समाजों में यह गतिरोध आते रहे हैं, वहां सहज विकास बाधित हुआ है.
उपन्यास : अपने-अपने कुरुक्षेत्र
रचनाकार : मीनाक्षी नटराजन
प्रकाशक : सामयिक प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली
मूल्य : रुपये 250 (पेपरबैक)
वरिष्ठ कथाकार महेश दर्पण के सात कहानी संग्रह, एक यात्रा वृत्तांत, पांच जीवनवृत्त और कई अन्य विधाओं में पुस्तकें आ चुकी हैं. कन्नड़ उर्दू, पंजाबी, मलयाली और रूसी भाषा में रचनाओं का अनुवाद हो चुका है. उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है.
Follow NRI Affairs on Facebook, Twitter and Youtube.